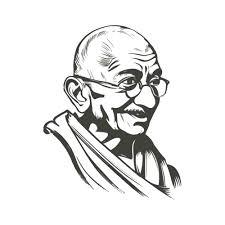निलेश देसाई
भोपाल। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक ही नहीं, बल्कि विश्वमानवता के भी पथप्रदर्शक रहे हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, आत्मानुशासन और नैतिक राजनीति का प्रयोगशाला था। परंतु यह भी सच है कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक गांधी पर असहमति और आलोचना के स्वर लगातार उठते रहे हैं। आलोचना किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है, किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब आलोचना से आगे बढ़कर गांधी को पूरी तरह नकारने या उनकी नियत पर प्रश्नचिह्न लगाने की प्रवृत्ति समाज में गहराने लगती है। यही प्रवृत्ति हमें यह समझने पर विवश करती है कि आखिर गांधी को नकारने की यह मानसिकता क्यों जन्म ले रही है और यह हमारे समाज के बदलते मानस की कौन-सी तस्वीर पेश करती है।
असहमति और निषेध का फर्क
गांधी के समकालीन नेताओं—नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. भीमराव आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या यहां तक कि जिन्ना तक—ने भी उनके कई निर्णयों पर असहमति जताई थी। यह असहमति विचारों की विविधता और लोकतांत्रिक विमर्श का अंग थी। लेकिन असहमति और निषेध में बड़ा अंतर है। असहमति का मतलब है विचार या रणनीति से असहमत होना, जबकि निषेध का अर्थ है किसी व्यक्तित्व की संपूर्ण उपस्थिति, योगदान और नियत को ही संदेह की दृष्टि से देखना। आज जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वह दूसरे प्रकार की है।
गांधी को नकारने के मनोवैज्ञानिक कारण
गांधी को नकारने की प्रवृत्ति केवल वैचारिक मतभेद से नहीं, बल्कि समाज की गहरी मनोवैज्ञानिक स्थितियों से भी जुड़ी है।
हीरो डिमोलिशन सिंड्रोम – समाज जब किसी नायक को अत्यधिक ऊँचाई पर पहुंचा देता है, तो समय-समय पर उसे गिराने की कोशिश भी करता है। इसे “हीरो डिमोलिशन सिंड्रोम” कहा जा सकता है। गांधी के साथ भी यही हुआ।
असफलताओं का बोझ अतीत पर डालना – जब वर्तमान समाज जटिल समस्याओं से जूझता है और समाधान तुरंत नहीं मिलता, तो लोग अतीत के नायकों को दोष देने लगते हैं। गांधी पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने देश के बंटवारे को रोका नहीं या कि वे मुसलमानों के पक्षधर थे, इसी मानसिकता का परिणाम है।
ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति – आज के दौर में विचारधाराएँ केवल तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं और पहचान की राजनीति पर खड़ी होती हैं। ऐसे माहौल में गांधी जैसे “समन्वयकारी व्यक्तित्व” को नकारना आसान प्रतीत होता है।
समाज का बदलता मानस
भारत का समाज समय के साथ तेज़ी से बदल रहा है। उपभोक्तावाद, तकनीकी विकास और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने लोगों की सोच को तात्कालिक और परिणामोन्मुख बना दिया है। गांधी का मार्ग, जो धैर्य, आत्मानुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि पर आधारित था, इस तेज़-तर्रार दौर में कई बार “धीमा” या “अप्रासंगिक” लगने लगता है। यही कारण है कि कुछ वर्ग गांधी के विचारों को पुराना मानकर खारिज करने की कोशिश करते हैं।
साथ ही, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहां किसी भी महान व्यक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यह स्वस्थ भी है, लेकिन जब यह चुनौती “तर्कसंगत आलोचना” से हटकर “पूर्ण अस्वीकार” का रूप लेने लगे, तब यह समाज की असुरक्षा और असंतोष का प्रतीक बन जाती है।
गांधी और आरएसएस की आलोचना की तुलना
दिलचस्प बात यह है कि ऐसी प्रवृत्ति केवल गांधी तक सीमित नहीं है। आरएसएस के संदर्भ में भी यही पैटर्न दिखता है। कुछ लोग उसके विचारों और नीतियों की आलोचना करते हैं, जबकि कुछ उसकी संपूर्ण उपस्थिति को ही नकार देते हैं। यानी किसी संस्था या व्यक्ति से असहमत होना और उसे पूरी तरह खारिज करना, दोनों में वही फर्क है जो गांधी के मामले में देखने को मिलता है। यह तुलना बताती है कि यह केवल किसी एक व्यक्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति है।
गांधी का मूल्यांकन कैसे हो?
गांधी को समझने का सही तरीका यह है कि हम उनकी गलतियों को स्वीकार करें, उनके निर्णयों पर बहस करें, परंतु उनकी नियत और ईमानदारी पर सवाल न उठाएँ। गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि वे “सत्य की खोज में एक प्रयोगकर्ता” हैं और उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यही था कि वे पारदर्शी थे, आत्मालोचना करते थे और गलती मानने में संकोच नहीं करते थे।
भविष्य के लिए संदेश
गांधी को नकारने की प्रवृत्ति दरअसल हमारे लोकतांत्रिक समाज के भीतर बढ़ते असहिष्णुता और मानसिक असुरक्षा का प्रतीक है। अगर यह प्रवृत्ति गहरी होती गई, तो समाज केवल अतीत के नायकों को गिराने में व्यस्त रहेगा और भविष्य के लिए ठोस समाधान नहीं खोज पाएगा। गांधी को नकारने की बजाय हमें यह समझना होगा कि उनका संदेश—सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और पारदर्शिता—आज की चुनौतियों जैसे जलवायु संकट, असमानता और हिंसा में भी उतना ही प्रासंगिक है।
गांधी को नकारने की मनोवृत्ति समाज के बदलते मानस की एक झलक अवश्य है, लेकिन यह हमारे लिए चेतावनी भी है। असहमति और आलोचना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं, किंतु संपूर्ण निषेध हमारी वैचारिक परंपरा को कमजोर करता है। गांधी को इतिहास के पन्नों तक सीमित करने या उन्हें विवादों में घसीटने से अधिक ज़रूरी यह है कि हम उनकी आत्मा को समझें और अपने समय की समस्याओं में उनके विचारों को सार्थक रूप से लागू करें।
गांधी को नकारना आसान है, परंतु उनके बताए रास्ते पर चलना कठिन। शायद यही कठिनाई हमें उनकी ओर बार-बार लौटने को बाध्य करती है।