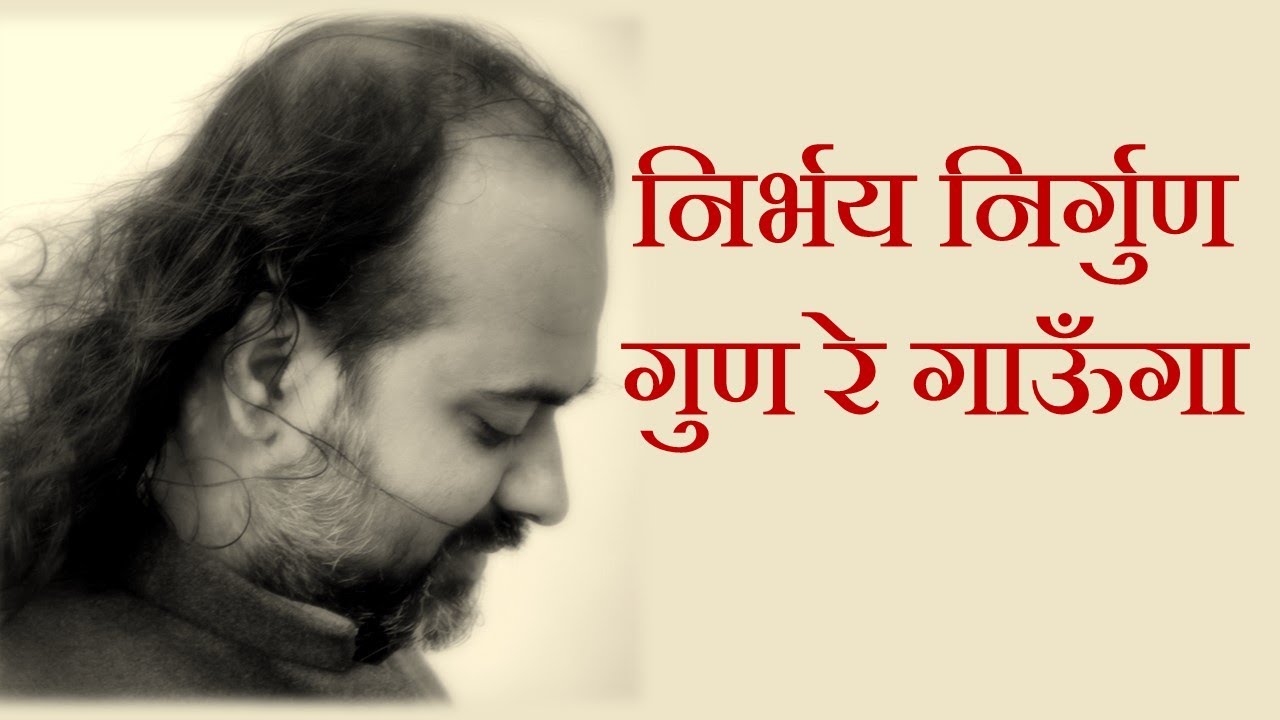हेमंत शर्मा
व्यक्ति के भीतर कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब वो स्तब्ध हो जाता है. इस स्तब्धता का कारक उसकी चेतना, क्षमता, कौशल, अभिव्यक्ति और गति को हर लेता है. हम रुक जाते हैं. चाहते हैं कि कहें, बोलें, चलें, लिखें, पर होता कुछ नहीं. कुछ क्षणों के लिए एक शांत नीरवता में गति का ज्वालामुखी लिए व्यक्ति बंध जाता है. मेरे लिए ऐसी स्थिति अक्सर अपने पिताजी और अपने गुरू प्रभाष जी के बारे में लिखने से पहले होती है. ऐसा लगता है कि मैं घाट पर दिया लिए सूर्य को प्रकाश दिखाने की गुस्ताखी कर रहा हूं. कलम रुकी हुई होती है. आंखों खोई हुई और मन-मस्तिष्क में अनंत घटनाएं, संदर्भ और तस्वीरें बहुत तेजी से उमड़ने-घुमड़ने लगती हैं. संतों पर लिखना थोड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि संत के बारे में आप जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके बारे में जानना शेष रह जाता है. यह अशेष एक किस्म का रहस्य पैदा करता है. उनका आभामंडल इतना विस्तृत होता है, जिसमें सारा संसार छोटा पड़ जाए. हम दुनियावी लोग उनके सामने सिर्फ श्रद्धा से सिर झुका सकते हैं.
प्रभाष जी के व्यक्तित्व का आकलन ‘जनसत्ता’ के बिना नहीं हो सकता. लोक चेतना की उनकी समझ और उनका प्रतिबद्ध व्यक्तित्व ही उन्हें सबसे अलग करता है. उनमें प्रतिबद्धता के साथ एक निःस्वार्थ दृढ़ता भी थी. वे संयमी, त्यागी, तपस्वी, निर्भीक और अपने आदर्शों को वहन करने वाले थे. अब कम लोग हैं जो इन मानकों पर खरे उतरते हों इसलिए जनसत्ता केवल अख़बार नहीं था, पत्रकारिता और समकालीन राजनीति का जीवंत इतिहास था. और प्रभाष जी उसके इतिहासकार.
लोक की नब्ज, सामाजिक सरोकार, टकसाली भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी की पाठशाला था जनसत्ता.
जिसने जनसत्ता में काम नहीं किया, उसे नहीं पता अख़बार की आजादी का मतलब.
प्रभाष जी को मैंने पत्रकारिता के संत के रूप में देखा. अखबार की दुनिया का एक मलंग साधु, जो धूनी रमाए सत्यं शिवं सुंदरम् के अनुसंधान में लीन है. उनके साधुत्व में एक शिशु-सी सरलता थी, उनकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ करुणा-स्नेह की गंगा थी, उनके अद्भुत स्पर्श से मुझ जैसों को लुकाठी हाथ में लेकर सच कहने और सच के लिए किसी से मुठभेड़ करने की हिम्मत और ताकत मिलती थी. प्रभाष जी कबीर और कुमार गंधर्व के नजदीक किसी और वजह से नहीं, बल्कि अपनी अक्खड़ता और फक्कड़ता के कारण थे.
प्रभाष जोशी होने का मतलब उसे ही समझाया जा सकता है, जो गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, कबीर, कुमार गंधर्व, सीके नायडू और सचिन तेंदुलकर होने का मतलब जानता हो. प्रभाष जी इन सबसे थोड़ा-थोड़ा मिलकर बने थे. यानी उनमें तेजस्विता, अक्खड़ता, सुर, लय, एकाग्रता और संघर्ष का अद्भुत समावेश था. कुमार गंधर्व की षष्ठिपूर्ति पर प्रभाष जी ने लिखा था, उस प्रभाष जोशी के भाग्य से कोई क्या ईर्ष्या करेगा, जिसकी सुबह कुमार जी की भैरवी से, दोपहर आमीर खाँ की तोड़ी से और शाम सीके नायडू के छक्के से होती है. प्रभाष जी देवास के अपने गांव आष्टा से कुछ बनने नहीं निकले थे, गांधी का काम करने घर से निकले थे. रास्ते में विनोबा मिले. अक्षर-पथ पर राहुल बारपुते मिले. कुमार गंधर्व की सोहबत मिली, ‘गुरुजी’ विष्णु चिंचालकर का साथ मिला. शब्द और सच के संधान में ‘प्रजानीति’ और ‘सर्वोदय’ से होते हुए उन्हें रामनाथ गोयनका मिले. गोयनका ने उन्हें एक्सप्रेस में बुलाया. और फिर देश व हिंदी समाज ने जाना प्रभाष जोशी होने का मतलब.
प्रभाष जी में ऐसा क्या था, जो उन्हें खास बनाता था? गर्व, हौसला और मुठभेड़. उन्हें अपनी परंपरा पर गौरव था. हिंदी समाज पर गर्व था. वे लगातार हिंदी समाज के सम्मान और उसके लेखक की सार्वजनिक हैसियत के लिए अभियान छेड़े हुए थे. और मुठभेड़…बिना मुठभेड़ के प्रभाष जी के जीवन में गति और लय नहीं होती थी. अक्सर बातचीत में वे कहते कि आजकल अपनी मुठभेड़ फलां से चल रही है. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, विश्व हिंदू परिषद, बाबरी विध्वंस, अर्थव्यवस्था या फिर उदारीकरण, कुछ नहीं तो पत्रकारिता में आई गिरावट ही सही. प्रभाष जी हर वक्त किसी न किसी से मुठभेड़ की मुद्रा में होते थे. आखिर कौन सी ताकत थी उनमें, जो पूरा देश एक किए रहते थे. आज मणिपुर में, कल पटना में फिर वाराणसी में… हर वक्त ढाई पग में पूरा देश नापने की ललक थी उनमें. सोचता हूँ कि एक पेसमेकर के भरोसे उन्होंने ढेर सारे मोर्चे खोल रखे थे. वे गांधीवादी निडरता के लगभग आखिरी उदाहरण थे. यही वजह थी कि 25 साल की डायबिटीज, एक बाईपास सर्जरी, एक पेसमेकर के बावजूद प्रतिबद्धता की कलम और संकल्पों का झोला लिए वे हमेशा यात्रा के लिए तैयार रहते थे. प्रभाष जी का नहीं रहना एक बड़े पत्रकार का नहीं रहना मात्र नहीं है. उनका न रहना मिशनरी पत्रकारिता का अंत है. चिंतन-प्रधान पत्रकारिता का अंत है. सच के लिए लड़ने और अड़ने वाली पत्रकारिता का अंत है. वे पत्रकारिता में वैचारिक विमर्श लौटाने की कोशिशों में लगे रहे. शायद इसी वजह से लोक संस्कृति-साहित्य और संगीत पर पहली बार जनसत्ता में एक-एक पेज उन्होंने अलग से तय किए थे.
हमें मालूम है कि हर युग में विरोध के अपने खतरे हैं. उन्हें भी मालूम था. उस कद के संपादक की माली हालत आप भी देख सकते हैं. दो मौकों पर उन्होंने राज्यसभा की मेम्बरी सिर्फ इसलिए ठुकराई कि उन्होंने विरोध के रास्ते पर चलना मंजूर किया था. कभी सत्ता-प्रतिष्ठान से जुड़ने की रत्ती भर इच्छा नहीं रही. वे कबीर की तरह हमेशा प्रतिपक्ष में रहे. बड़वाह में उनके अंतिम संस्कार के वक्त नर्मदा के किनारे चिता पर प्रभाष जी की देह थी और आकाश में ‘अमर हो’ की गूंज. सामने खड़ा मैं सोच रहा था कि इस पांच फीट दस इंच के शरीर के जरिए आखिर क्या छूट रहा है? जवाब स्वयं से आया कि पत्रकारिता की एक पूरी पीढ़ी छूट रही है. एक संकल्पबद्ध कलम छूट रही है. वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करने वाला एक विचार छूट रहा है. भाषा को लोक तक पहुंचाने वाला एक शैलीकार छूट रहा है. अदम्य साहस और निडरता से किसी सत्ता प्रतिष्ठान से मुठभेड़ करने वाला एक योद्धा छूट रहा है. लोक और समाज के गर्भनाल रिश्तों की तलाश करने वाला एक समाज विज्ञानी छूट रहा है. जनसत्ता के जरिए समकालीन पत्रकारिता में एक पूरी पीढ़ी देने वाला छूट रहा है. हम छूट रहे हैं. पत्रकारिता में ‘निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा’ की जिद छूट रही है. प्रभाष जी अपने पसंदीदा गायक कुमार गंधर्व के इस गीत को ताउम्र सुनकर रीझते रहे. मृत्यु के बाद भी जलती चिता के पास उनके भाई और बेटी सोनल वही भजन गाकर उन्हें सुना रहे थे.
जो लोग प्रभाष जी को नहीं जानते, वे उन्हें वामपंथी, नास्तिक और निरा धर्म-विरोधी मानते हैं. प्रभाष जी अपनी आस्तिकता को कभी छुपाते नहीं थे. परम वैष्णव प्रभाष जी सिर्फ धर्म के पाखंड का विरोध करते थे. मृत्यु से कुछ साल पहले श्रावण मास में वैद्यनाथ धाम जा पहले कांवर को देवघर के लिए रवाना करने वाले प्रभाष जी ही थे. पूरे कुटुम्ब को इकट्ठा कर वृंदावन में कई दिनों रहना, फिर सबको लेकर नाथद्वारा जाना उन्हें अच्छा लगता था. प्रभाष जी का मानना था कि धर्म के जरिए और धर्म में रहकर ही धार्मिक पाखंडियों से लड़ा जा सकता है. धर्म को छोड़कर और हिंदुओं को गाली देकर हम छद्म हिंदुत्व से नहीं निपट सकते. इसलिए इनसे वामपंथी नहीं लड़ सकते. मालवा के रीति-रिवाज उनके संस्कार में थे. नर्मदा से उन्हें बेहद प्यार था. नर्मदा उनके दिल में बसी थी. ‘धन्न नरबदा मइया हो’ के लेखक की अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनका अंतिम संस्कार नर्मदा के किनारे ही हो. और हुआ भी ऐसा.
‘जनसत्ता’ के ज़रिए प्रभाष जी ने हिंदी अखबारों के लिए नई भाषा गढ़ी, शैली दी. सच पूछिए तो वे हिंदी अखबारों के शैलीकार थे. उन्होंने भाषा को लोक से जोड़ा. उसकी जड़ता खत्म की. वर्तनी का एक मानक तैयार किया. इससे पहले हिंदी अखबारों के संपादकीय पेज अंग्रेजी का उथला अनुवाद होते थे. जोशी जी ने उसका चलन बदला, उसे तेवर दिया. हिंदी समाज को स्वाभिमान दिया. तब तक हिंदी को झोलाछाप पत्रकारों का कुनबा माना जाता था.
सच यह है कि आज हिंदी के हर अखबार के पन्नों पर प्रभाष जी की भाषा की मुहर है. आतंकवादियों के लिए ‘खाड़कू’, फिदायीनों के लिए ‘मरजीवड़े’, भ्रष्ट राजनेताओं के लिए ‘चिरकुट’ शब्द प्रभाष जी ने गढ़े. इससे पहले अखबारों में शब्द गढ़ने का काम पराड़कर जी ने किया था. और यही भाषा जब उनके ‘कागद कारे’ कॉलम के निजी लेखों में प्रवाह बनाती है तो कुबेरनाथ राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद व्यक्तिव्यंजक निबंधों का विस्तार दिखता है. उनकी सृजनात्मकता का अमोघ अस्त्र थी उनकी भाषा. नामवर सिंह के शब्दों में– ‘ठेठ हिंदी का ठाठ’ क्या है, इसका अहसास प्रभाष जी का गद्य पढ़ने से होता है. उनका गद्य हाथ कते, हाथ बुने, हाथ सिले खादी के परिधानों की तरह और तुलसी के शब्दों में ‘विशद गुनमय फल’ वाला है. जिस अंदाज में प्रभाष जी क्रिकेट पर लिखते थे, उसी रंग में क्या साहित्यिक कृतियों पर लिखा जा सकता है, यह चुनौती रखी प्रभाष जी ने हिंदी गद्यकारों के सामने.
प्रभाष जी ने हमें बताया कि पत्रकारिता करने और करके दिखाने की चीज है. सिर्फ उपदेश देने या सिखाने की नहीं. प्रभाष जी महज़ गांधीवादी नहीं थे. उन्होंने गांधी के विचारों को जिया भी था. इससे मिलने वाले नैतिक बल ने ही उन्हें इंदिरा गांधी जैसी सबसे ताकतवर सत्ता-प्रतिष्ठान के खिलाफ डटे रहने की हिम्मत दी. अखबारी आजादी के वे कायल थे और अखबारों में घुसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वे उसी ताकत से लड़ते थे. खासकर तब जब आर्थिक उदारीकरण के बाजार ने उसे डसा. खबरों को लकवा लगा. खबरें बेचने और खरीदने का तंत्र विकसित हुआ. प्रभाष जी ने हिंदी अखबारों में पैसे लेकर खबर छापने के खिलाफ मोर्चा खोला. कहा, पत्रकारिता बचेगी तो देश बचेगा. पहले पत्रकारिता को तो बचा लें. इसलिए अभी राजनेताओं से निपटने से पहले उनसे मुठभेड़ जरूरी है. मृत्यु से एक रोज पहले लखनऊ-बनारस की जिस यात्रा से वे लौटे थे, वह इसी अभियान का हिस्सा थी. चुनावी खबरों को पैकेज की तर्ज पर बेचने के खिलाफ हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल में उन्होंने निगरानी कमेटियां बनाई थीं. जोशी जी अभी पत्रकारिता की पवित्रता को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे थे. लड़ाई तो शुरू ही हुई थी. बाजार के राक्षस से उनकी मुठभेड़ चलनी थी. उनके असमय अवसान से यह अभियान रुक गया.
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजकल के बोनसाई संपादकों की जमात के मुकाबले वे अकेले और अंतिम संपादक थे. पत्रकारिता को सरोकारों से जोड़ने, मुद्दों पर तनकर और डटकर खड़े होने वाले, जिनके हाथ में कलम, पैर में परंपरा, दिल में गांधी और कबीर और दिमाग में भ्रष्ट तंत्र और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जूझने के औजार गढ़ने का सामर्थ्य था. संपादक तो बहुत हुए, पर कोई बता दे ऐसा संपादक जिसने हिंदी पत्रकारिता को पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी दी. इस पीढ़ी को उन्होंने अपने हाथों गढ़ा, चलना सिखाया, अड़ना सिखाया और सरोकारों से जुड़ने का मकसद दिया. लोगों के बीच जाकर संवाद कायम किया. चाहे नर्मदा बचाने का सवाल हो या सूचना पाने का अधिकार हो या फिर खबरों की खरीद-फरोख्त का मामला- प्रभाष जी इस लड़ाई में सबसे आगे रहे. हालांकि उनकी यह जिद ‘प्रोफेशनल’ लोगों को रास नहीं आई. खासकर पूंजीपतियों के सलाहकार टाइप संपादकों को, जो सुविधाओं के झूले में झूलते-झूलते वैचारिक नपुंसकता को प्राप्त कर गए. ये लोग भूल जाते हैं कि प्रभाष जी अपने वक्त में अखबार मालिकों के प्रिय व करीबी रहे. चाहे वे ‘नई दुनिया’ के राहुल बारपुते हों या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के रामनाथ गोयनका. लेकिन उन्होंने कभी अपने संपादक पर अखबार मालिकों को सवार नहीं होने दिया. जो गोयनका अपने संपादकों को ताश के पत्तों की तरह फेंटने के लिए कुख्यात थे, गालियों से बात करने के अभ्यस्त थे, वे भी प्रभाष जी से शराफत से पेश आते थे. वे अखबारों में दखल नहीं देते थे. अखबार मालिकों को काबू करने के लिए जोशी जी के औजार और थे. अब वे औजार सुविधा और चाटुकारिता के हैं.
हमने अपने जमाने के कई संपादक देखे. पर जोशी जी जितना ताकतवर संपादक हिंदी और अंग्रेजी में नहीं हुआ. उनके सामने प्रबंधन तो झुकता ही था, पाठक भी न्योछावर थे. कितने अखबार और संपादक इतने सौभाग्यशाली होंगे जो अखबार छापने के चंद दिनों बाद ही पाठकों से निहोरा करें कि अब अखबार खरीदकर नहीं, मिल-बांटकर पढ़ें, क्योंकि हमारी मशीन इससे ज्यादा अखबार छाप नहीं सकती हैं. खास बात यह है कि तब तक पत्रकारिता में बाजार दस्तक दे चुका था और विज्ञापनों में अखबारों की प्रसार संख्या का महत्त्व था. ऐसे में जोशी जी पाठकों से अपील कर रहे थे कि जनसत्ता खरीदकर नहीं बल्कि मिल बॉंट कर पढ़िए.
जनसत्ता के प्रभाष जोशी को समझने के क्रम में अयोध्या का जिक्र भी ज़रूरी है. अयोध्या कांड से देश की राजनीति ने करवट बदली. साथ ही प्रभाष जी की लेखनी और व्यक्तित्व ने भी. अयोध्या मामले से दो बातें साफ होती हैं. प्रभाष जी लिखने की आजादी के किस हद तक पक्षधर रहे. क्या कोई संपादक संपादकीय लेखों और खबरों में अलग-अलग लाइन की छूट दे सकता है? दूसरी बात यह कि विश्व हिंदू परिषद से प्रभाष जी आखिर क्यों नाराज हो गए और अंत तक ललकारते रहे. यह अब तक लोगों के लिए अबूझ पहेली है. इस बारे में तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हैं. पर यह सवाल मौजूं है कि जो प्रभाष जोशी संघ परिवार और नरसिंह राव के बीच अयोध्या मामले में बातचीत का हिस्सा थे, वे आखिर क्यों संघ परिवार पर फट पड़े? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो जमात कल तक सती प्रथा पर सिर्फ एक लेख लिखने की वजह से प्रभाष जी को पोंगापंथी कहने लगी थी, वही रातोरात प्रभाष जी को अपने पाले में ले उड़ी. इन सवालों का खुलासा राजनीति का अयोध्या कांड करता है.
6 दिसंबर 1992 को जब मैंने अयोध्या के एक पीसीओ से प्रभाष जी को बाबरी ध्वंस की जानकारी देने के लिए फोन किया तो राम बाबू ने कहा, ‘संपादक जी आपको ढूंढ़ रहे हैं’. राम बाबू संपादक के निजी सचिव थे. मैंने प्रभाष जी को बाबरी ध्वंस की पूरी कहानी बताई. प्रभाष जी रोने लगे. कुछ देर चुप रहे. फिर कहा, ‘यह धोखा है, छल है, कपट है. यह विश्वासघात है. यह हमारा धर्म नहीं है. अब हम इन लोगों से निपटेंगे.’ प्रभाष जी विचलित थे. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं दोपहर बारह बजे से शाम पांच बजे के ध्वंस का पूरा हाल पांच मिनट में उन्हें सुनाने की रिपोर्टरी उत्तेजना में था. उनका मानना था कि ये हिंदुत्ववादी हिंदू धर्म से कोसों दूर थे जो बाबरी ढांचे को ढहा रहे थे. इन्होंने धर्म की मर्यादा, सहिष्णुता, वैष्णवता और उदारता को ध्वस्त किया है. शायद इसलिए जनाक्रोश के उभार के बावजूद वे हिंदी के अकेले संपादक थे, जिन्होंने अपना अलग ‘स्टैंड’ लिया. बाकी हिंदी अखबार कारसेवा में बह गए.
नतीजतन प्रभाष जी ने मुझे ‘रामभक्त’ पत्रकार घोषित कर दिया. उसी अखबार में अपने लेखों में मुझे इस नाम से संबोधित किया. मेरी खबरों को खारिज करते हुए संपादकीय लिखे. एक उदाहरण, कार्तिक पूर्णिमा पर विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में संकल्प आयोजन रखा. मैंने रपट लिखी. ‘आज पांच लाख लोगों ने सरयू तट पर डुबकी लगाई और मंदिर निर्माण का संकल्प लिया’ आदि-आदि. मेरी यह खबर पहले पेज पर छपी. दूसरे दिन प्रभाष जी का लेख छपता है कि मेरे रामभक्त पत्रकार ने लिखा है कि कल अयोध्या में पांच लाख लोगों ने सरयू तट के किनारे मंदिर निर्माण का संकल्प लिया. मैं उन्हें बता दूं कि अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के रोज डुबकी लगाने वाले सभी लोग विहिप के सदस्य नहीं हैं. अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान की यह परंपरा तब से चल रही है जब विहिप, संघ और उनके संस्थापकों का जन्म भी नहीं हुआ था. डुबकी का यह सिलसिला हमारी अनंत परंपरा में है. ऐसे कम से कम दस अवसर होंगे जब प्रभाष जी ने मुझे अपने लेखों के जरिए सचेत किया. लेकिन मेरी रिपोर्ट ‘किल’ कभी नहीं की. यह आजादी उन्होंने मुझे दी थी. फिर ऐसी आजादी कभी नहीं मिली.
मैं पूरे अयोध्या आंदोलन में प्रभाष जी की संपादकीय लाइन के खिलाफ था. प्रभाष जी चाहते तो हिंदी संपादकों की आज की परंपरा के तहत मुझे ही लाइन पर ले सकते थे. उनके पास चार विकल्प थे. एक- प्रधान संपादक के नाते वे मेरी खबरों को संपादित कराते. वह अंश निकाले जाते जिन पर उन्हें एतराज होता. दो- फिर भी नहीं मानता तो मेरी खबरें किल होतीं. जैसा बाद में एक संपादक ने रामबहादुर राय की कई रपटों के साथ किया. तीन- हेमंत शर्मा चेत जाओ, नहीं चलेगी तुम्हारी अराजकता. यह मेमो मिलता. और चार- मुझे नमस्कार कर घर बैठने को कहा जा सकता था. संपादकों की उत्तर प्रभाष जोशी परंपरा में चौथा विकल्प आजकल सबसे आसान है. आप कह सकते हैं, यह अराजक आजादी थी. पर थी. पर इसी आजादी ने जनसत्ता का चरित्र बनाया और जनसत्ता के प्रभाष जोशी को संपादकीय आजादी के शिखर पर पहुंचाया.
अपने रिपोर्टरों को ऐसी आजादी कौन देता है? कौन संपादक है आज, जो अपने रिपोर्टर के पीछे मजबूती से खड़ा हो. और मुद्दों पर उनके सामने उसी मजबूती से अड़ा हो. प्रभाष जी ने कभी भी कोई रिपोर्ट इसलिए नहीं रोकी कि रिपोर्ट संपादक को पसंद नहीं है. या इस रिपोर्ट से कोई राजनेता नाराज होगा या फिर फलां आदमी संपादक का मित्र है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने विवेकाधीन कोष से पत्रकारों को पैसे बांटे. 42 करोड़ की इस बांट में करोड़ों रुपए पत्रकारों में बंटे. खुसुर-फुसुर चल रही थी. राज्य में ऐसा माहौल लगा कि हर दूसरे पत्रकार ने पैसा लिया है. जनसत्ता ने सबसे पहले पैसा लेने वालों की सूची छापी. सूची में संपादक के एक मित्र वेद प्रताप ‘वैदिक’ जी का नाम भी छपा. हालांकि उन्हें यह रकम ‘अंग्रेजी हटाओ आंदोलन’ के लिए दी गई थी. मुलायम सिंह यादव भी इसी आंदोलन में शामिल थे. खबर छप गई. बवाल मचा. वैदिक जी ने तीन पेज की चिट्ठी लिखी. मेरे खिलाफ. मुझे बताया गया कि वैदिक जी संपादक के बचपन के दोस्त हैं. मैं क्या करता, तीर छूट चुका था. तीसरे दिन मुझे एक चिट्ठी मिली. चिट्ठी वैदिक जी की थी. जिस पर एक कोने में प्रभाष जी का आदेश लिखा था, ‘बिंदुवार जवाब दें- प्र.जो,’. मैंने जवाब दिया. लगा कुछ कार्रवाई होगी. तीन रोज बाद संपादकीय पेज पर वैदिक जी की चिट्ठी छपी. और उसके बगल में मेरा जवाब ‘वैदिक जी झूठ बोल रहे हैं’.
अब बात अयोध्या पर प्रभाष जोशी के बिफरने की. यह बहुत कम लोगों को पता है कि प्रभाष जी सरकार और संघ के बीच अयोध्या पर हो रही बातचीत का हिस्सा थे. कोई बीच का रास्ता निकले, सहमति बने, इस कोशिश में वे ईमानदारी से लगे थे. वे नरसिंह राव और रज्जू भैया के बीच होने वाली बातचीत में भी शामिल थे. होने वाली हर बातचीत में कुछ बातें साफ थीं. ढांचा गिराया नहीं जाएगा और सहमति बनने तक विवादित स्थल के बाहर कारसेवा की इजाजत दी जाएगी. 9 जुलाई से ढांचे के सामने जिस चबूतरे पर कारसेवा होनी थी उसके बारे में जनसत्ता पहला अखबार था जिसने लिखा कि कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर होगी कारसेवा. दूसरे रोज 8 जुलाई को फिर खबर दी- ‘झूठ और फरेब पर बनेगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर’. इसी रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जुलाई कोकारसेवा रोक दी. बावजूद इसके प्रभाष जी मुझे रामभक्त कहते रहे. मैंने कभी उनसे इसकी शिकायत भी नहीं की. यहीं से प्रभाष जी ने अपनी लाइन बदली.
इसी खुन्नस में चम्पुओं ने यह प्रचार शुरू किया कि उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा, इसलिए प्रभाष जी नाराज हैं. उन्हें यह पता ही नहीं कि जब 1989 में वीपी सिंह ने सरकार बनाई तो प्रभाष जी को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव हुआ था. लेकिन प्रभाष जी को उस रास्ते नहीं जाना था. सो वे नहीं गए. प्रभाष जी जेपी के सहयोगी रहे हैं. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और नरसिंह राव जैसे प्रधानमंत्रियों से उनकी मित्रता रही है. उनके लिए यह मामूली चीज थी. पर राजनीति उन्हें भायी नहीं. 1998 के सितंबर में मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सात रेसकोर्स पर मिला. मैं लखनऊ से आता था. अटल जी कल्याण सिंह सरकार में रुचि रखते थे, इसलिए मेरी उनसे लगभग हर दिल्ली यात्रा में बात होती थी. इस बार अटल जी ने यकायक कहा, ‘प्रभाष जी को क्या हो गया है.’ इस पर मैंने कहा कि आपके ही लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें राजसभा में नहीं भेजा इसलिए वे नाराज़ हैं. अटल जी ने छूटते ही कहा कि मैं यह नहीं मानता. प्रभाष जी इससे ऊपर हैं. मैं उनकी तकलीफ समझता हूं. लेकिन उनकी भाषा से सहमत नहीं हूं. मैं इस प्रसंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अटल जी भी इस प्रचार की असलियत समझते थे. दरअसल, बाबरी मस्जिद प्रभाष जी की नजरों में सिर्फ भारतीय मुसलमानों की ऐतिहासिक और अतिक्रमित धर्मस्थली नहीं थी. वह उनके लिए हिंदुओं की धर्म-संस्कृति और सामाजिक परंपराओं की कसौटी भी थी.
संपादक जी ने मुझे 1984 में काशी की पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जो लकड़ी सुंघाई तो आज तक उन्हीं का होकर रह गया. मैंने उस रोज पंचगंगा घाट पर गुरु पाया था. प्रभाष जी बनारस आए थे. मैं बीएचयू में हिंदी का शोध छात्र था. कुछ रपटें जनसत्ता में छपी थीं. मैं ताज होटल में उनसे मिलने पहुंचा. तड़के साढ़े तीन बजे आने का आदेश हुआ. अवाक था, तड़के साढ़े तीन बजे यह भी कोई मिलने का समय… बाद में पता चला कि काशी विश्वनाथ की मंगला आरती और गंगा दर्शन के लिए चलना था. हम काशी विश्वनाथ की आरती में समय से पहले पहुंच गए थे. इसलिए घाटों पर टहलते-टहलते पंचगंगा घाट पहुंचे. यकायक प्रभाष जी ने पूछा ‘बनारस में गंगा सबसे पवित्रतम स्थिति में क्यों है?’
मैं अवाक क्या बताऊं. बचपन से सुन रखा था. यहां गंगा उत्तरवाहिनी है. इसलिए पवित्र है. मैंने यह ज्ञान जस का तस उड़ेल दिया. वे बोले तो इससे क्या होता है. मैंने कहा, यहां गंगा उत्तर की ओर देख रही है. जब नदियां अपने मूल की ओर देखें तो पवित्र स्थिति होती है. प्रभाष जी ने कहा ‘आदमी तो समझदार हो पंडित. कोई भी अपने मूल की ओर देखे तो यह सुखद और पवित्र स्थिति होती है. उससे व्यक्ति को अपनी औकात का पता चलता रहता है. इसलिए अपनी जड़ों को देखते रहना चाहिए.’ मुझे गुरु मंत्र मिल गया था. संयोग से यह वही सीढ़ियां थीं. जहां सोलहवीं सदी में रामानंद ने कबीर को मंत्र दिया था. पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर ही कबीर चुपके से लेटे थे. क्योंकि रामानंद ने उन्हें शिष्य बनाने से मना कर दिया था. रात के अंधेरे में सीढ़ियां उतरते रामानंद के पांव कबीर की छाती पर पड़े. वे राम-राम कहते पीछे हटे. कबीर ने इसे ही ‘गुरु मंत्र’ माना. न हम कबीर न वे रामानंद. पर घाट पंचगंगा था. और हमें गुरु मिल गया. मंत्र था, ‘अपनी जड़ों को पहचानो. उससे हमेशा गर्भनाल संबंध बना रहे.’ और इस तरह बीएचयू में यूजीसी का एक फैलो, हिंदी का शोधार्थी प्रभाष जी की टोली का पत्रकार बन गया.
इस घटना के कोई दस साल बाद कलकत्ते से ‘जनसत्ता’ का संस्करण छपा. प्रभाष जी अखबार निकालने के लिए कलकत्ते में थे. मुझे लखनऊ फोन किया. ठसक वाली रोबदार आवाज में ‘पूछा’ क्या कहा था आपने. नदियां अपने मूल की ओर देखें या लौटें तो सबसे पवित्र होती हैं न. मैं कुछ समझा नहीं. ‘जी’ कह ही पाया था कि वे बोले, आज हिंदी पत्रकारिता अपने मूल पर लौट रही है. जनसत्ता आज से कलकत्ते से छपेगा. पत्रकारिता अपने स्रोत पर लौट आई है. जनसत्ता का यह संस्करण इस लिहाज से ऐतिहासिक है. दूसरे रोज संपादक जी का इन्हीं लाइन पर अग्रलेख भी पहले पेज पर था. आप जानते ही हैं कि हिंदी का पहला अखबार ‘उदंत मार्तंड’ 30 मई 1826 को कलकत्ते से ही छपा था.
दुनिया तेजी से बदलती जा रही है. उतनी ही तेजी से बदल रहा है हमारा समाज और समाज के संवाद का तरीका, पत्रकारिता. अखबारों की प्रसार संख्या सिमटती जा रही है. टीवी चैनल एकरूप और एकरस होकर अब निरस हो चले हैं. घरों में टीवी एक सामुहिक संचार था, वहां अब सास-बहू देखने वाली तादाद तक सिमटती जा रही है, खबरिया चैनलों की तो क्या ही बिसात. हिंदी और अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं एक अजीब से उत्तरजीवित्व संकट से गुज़र रही हैं. कई दम तोड़ चुकीं. कुछ दम बचाने के लिए रेंगती नज़र आ रही हैं. जन और सत्ता के बीच पत्रकारिता की जगह एक सामुहिक शोर ने ले ली है. इसे सोशल मीडिया कहते हैं. यहां न भाषा है, न मेहनत, न वस्तुनिष्ठता है और न जिम्मेदारी, जवाबदेही और नैतिकता का ख़याल भी अब बीते जमाने की बात जैसा माना जाने लगा है. पत्रकारिता अध्ययन संस्थानों में भेड़ों का झुंड तैयार किया जा रहा है जो इतिहास, भाषा, साहित्य, राजनीति और संस्कृति का अन्नप्रासन तक नहीं कर सके हैं और कैमराजीवी बनने की होड़ में जुटे हैं. संपादक जैसी संस्था तो खैर खत्म ही है तो फिर भाषा, लेखन, विषय, अध्ययन और समाज के लिए लड़ने का सवाल ही नहीं दिखता. कभी कभी कुछ लोग समाज के लिए बोलते नज़र आते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दरअसल स्वयं सिद्धि का ही स्वांग है, इसमें त्याग और संघर्ष दोनों की कमी है. और फिर इन सबको देखते हुए एक असहाय मन और चेतना को दिखता है वही मूलमंत्र- ‘उत्तरवाहिनी गंगा की ओर देखो, पंडित. जड़ों को पहचानो. मूल से जुड़ो’. प्रभाष जी जैसा भगीरथ जीवन… वो जो कह, लिख और बता कर गए हैं, वही उद्धार को व्याकुल हम जीवाश्मों को तार सकता है.
साभार