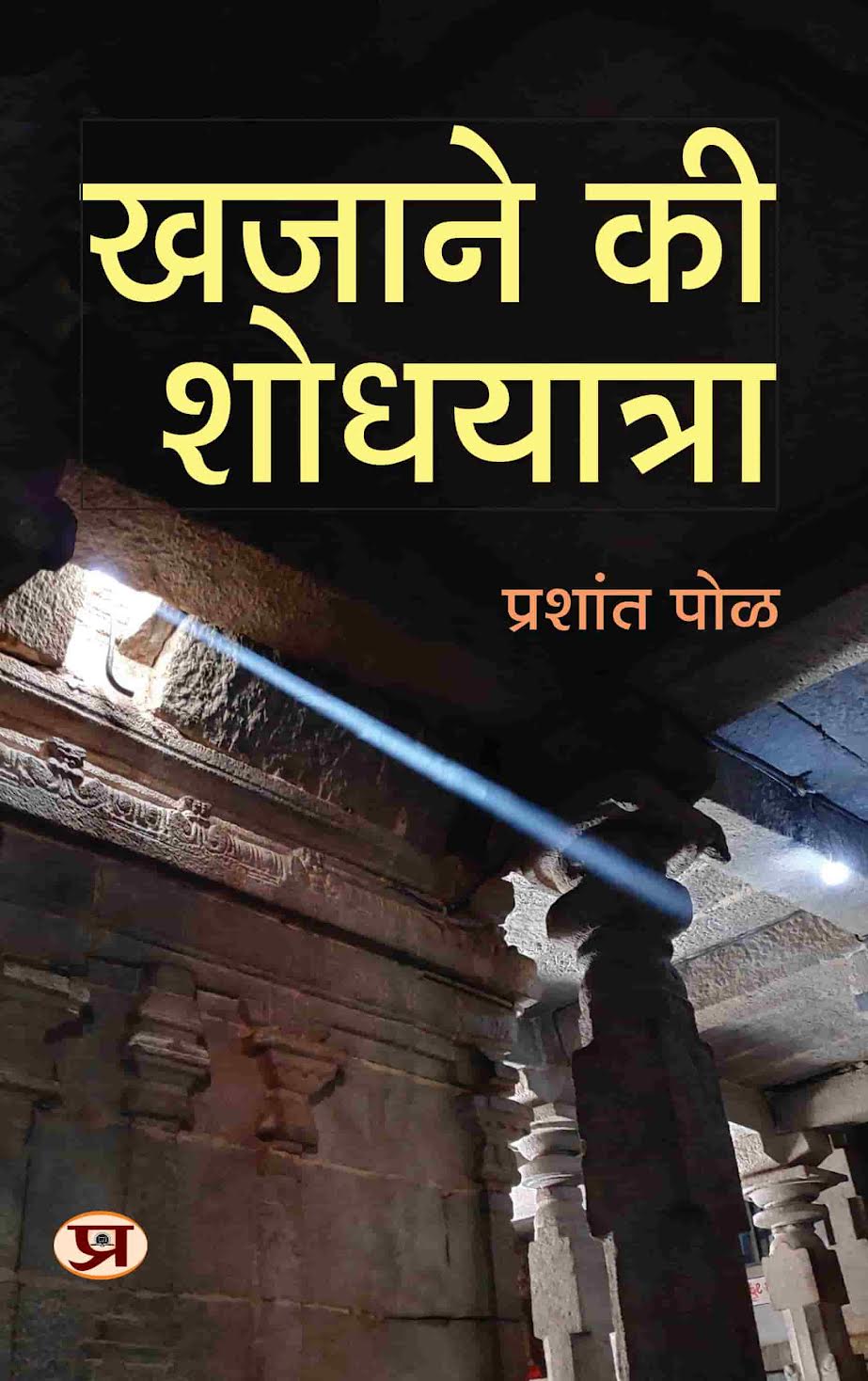प्रशांत पोळ
भारतीय ज्ञान का खजाना इस पुस्तक का मराठी संस्करण प्रकाशित हुआ, 14 मई 2017 को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केबिनेट मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल की उपस्थिति में यह भव्य समारोह, पुणे में संपन्न हुआ। मेरी यह पहली ही पुस्तक थी। इस पुस्तक में, आशीर्वाद के रूप में परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की प्रस्तावना थी।
मेरे लिए यह सुखद अनुभव था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अनेकों ने कहां, कि इसका दूसरा भाग भी आना चाहिए। कइयों ने तो इसके लिए मेरा फॉलोअप लिया।
लगभग 2015 से में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ इस विषय पर थोड़ा बहुत लिखने लगा। उन दिनों इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। माननीय सुरेश सोनी जी की दो पुस्तकें थी, जो इस विषय पर पढ़ने / लिखने के लिए प्रेरणा दे रही थी। पर इसके इतर, ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं था। अभी जो प्रचलन में है, वह ‘आईकेएस’ (इंडियन नॉलेज सिस्टम), यह शब्द तो बहुत दूर था। सोशल मीडिया पर भी उन दिनों ज्यादा कुछ नहीं मिलता था।
ऐसे में इस पुस्तक का जबरदस्त स्वागत हुआ। मराठी के अतिरिक्त यह हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई। अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की। सभी भाषाओं में, इसके अनेक संस्करण निकले और निकल रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने इसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में मान्यता दी हैं।
तो, ऐसे अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक का अगला भाग (सीक्वल) लिखना, यह मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी। *खजाने की शोधयात्रा* लिखते समय इसकी पूरी गंभीरता मुझे थी।
अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध हैं, कि विषयों की कमी नहीं थी। बस, ज्यादा से ज्यादा शोध करना; प्रमाणिक, वास्तविक और अधिकृत संदर्भ ढूंढना, उन्हें सत्यापित करना, यह बहुत बड़ा काम था। अनेक बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़े। संस्कृत को समझना पड़ा। अनेक संदर्भ खोज कर निकालने पड़े… ऐसा बहुत कुछ।
पर यह सब करते हुए बड़ा मजा आया। आनंद आया। यह मेरा प्रिय विषय हैं। पसंदीदा हैं। इसलिए, इस विषय से संबंधित पुस्तकों में / ग्र॔थों में अवगाहन करना, यह एक आनंदमयी अनुभव था। पुस्तक लिखने के इस पूरे प्रवास में मैंने इस आनंद का भरपूर अनुभव लिया।
*यह सब अभ्यास करते समय मुझे बार-बार यह अनुभूति होती थी, कि हमारी ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध और संपन्न हैं। हम उन दिनों तत्कालीन दुनिया से बहुत आगे थे। ग्यारहवीं – बारहवीं सदी में, यदि इस्लामी आक्रांता भारत नहीं आते, तो शायद भारत ही नहीं, अपितु विश्व का इतिहास और भूगोल, दोनों बदले हुए रहते।*
यह पुस्तक लिखते समय, ‘पुराना हैं, तो ही सब सुहाना हैं’ या, ‘मात्र भारतीयों के पास ही सब कुछ ज्ञान था’ यह मेरी भूमिका नहीं थी। यह उचित भी नहीं हैं। किंतु यह भी सत्य हैं, कि कुछ हजार वर्ष, अपना भारत विश्व में सर्वाधिक समृद्ध, संपन्न और ज्ञानवान देश था।
*भारत में ‘भाष्य’ की परंपरा सनातन हैं। इसलिए, देश-काल-परिस्थिति के अनुसार, परिवर्तन होते रहेंगे, संकल्पनाएं बदलती रहेंगी, ज्यादा अच्छी चीजों का शोध सतत लगता रहेगा, नई तकनीकी आती रहेगी.. इन सारी बातों पर अपने पूर्वजों की दृढ़ श्रद्धा थी। आद्य शंकराचार्य समवेत अनेकों ने, लगभग प्रत्येक विषय पर भाष्य लिखे। इसके कारण अनेक नई बातें सामने आती गई। सारे विश्व में अपनी ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ रही, कारण भाष्य के रूप में, प्रत्येक सिद्धांत का, प्रत्येक संकल्पना का, खंडन – मंडन करते हुए आगे जाना, यह हमारे समाज का स्थाई भाव रहा हैं।*
ऋग्वेद के एक सूक्त पर भाष्य लिखकर, विजयनगर साम्राज्य के सायणाचार्य ने प्रकाश के वेग की सटीक गणना की, तो आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर जीवन के मूल्य, दैनिक व्यवहार के नियम, व्यवस्थापन के सिद्धांत आदि विषयों की नए सिरे से व्याख्या की। न्यायशास्त्र के कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति जैसे ग्रंथों पर अनेक भाष्य लिखे गए और अपने देश में स्थल-काल-परिस्थिति अनुरूप, न्यायव्यवस्था विकसित होती गई।
*विश्व के इतिहास में, दूसरे किसी धर्म में, राष्ट्र में या व्यवस्था में, इस प्रकार की ‘कंटीन्यूअस करेक्शन मेकैनिज्म’ अस्तित्व में नहीं हैं..!*
खजाने की शोधयात्रा इस पुस्तक में इन सब बातों की समीक्षा की हैं। सूर्य मंदिरों की अद्भुत रचना से लेकर तो भारत की प्राचीन और परिपूर्ण न्यायव्यवस्था तक, अनेक विषय इस पुस्तक में लेने का प्रयास किया हैं। प्राकृतिक खेती पर हमारे पुरखों ने कितना गहन विचार किया था, यह इस विषय पर अभ्यास करते हुए समझ में आया। पिंगल ऋषि ने आज के कंप्यूटर / डिजिटल प्रणाली का आधार, ‘बाइनरी सिस्टम’, का भी विचार करके रखा था। आज की कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) यह मानवी मन का शोध लेते समय, ‘भाषा’ इस माध्यम का उपयोग करती हैं। इस भाषा का मानवी मन (बुद्धि) के संदर्भ में पाणिनि ने किस प्रकार से विचार किया था, यह देखकर हम दंग रह जाते हैं..!
*खजाने की शोधयात्रा* के निमित्त, अक्षरश: हजारों संदर्भ देखें। पढे। उनका अध्ययन किया। किंतु यह सब करते हुए एक बात दिल को कचोट रही थी, कि अपनी इस समृद्ध ज्ञान परंपरा पर अपने भारतीयों ने ज्यादा शोध नहीं किए हैं। इन विषयों पर न तो ज्यादा प्रबंध हैं, और न हीं पीएचडी। इसलिए संदर्भों के लिए, कई बार विदेशी खोजकर्ताओं के संदर्भों की ही मदद लेनी पड़ती हैं। समरांगण सूत्रधार, बृहत्संहिता जैसे ग्रंथों के लिए, अधिकतर संदर्भ विदेशी शोधकर्ताओं के ही मिलते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य हैं।
यह सब अभ्यास करते समय मन में बार-बार प्रश्न निर्माण हो रहा था, कि कृषि पाराशर, वृक्षायुर्वेद, बृहत्संहिता, समरांगण सूत्रधार, ब्राह्मस्फूट सिद्धांत, न्याय कंदली, सहदेव भाळकी, कात्यायन स्मृति, युक्ति कल्पतरु… जैसे ग्रंथों पर, अपने विश्वविद्यालयों में ज्यादा शोध न होने का कारण क्या हैं? इन विषयों पर पीएचडी करने की कोई सोचता क्यों नहीं हैं..? मुझे विश्वास हैं, इन शोध के प्रयासों से, अनेक नई और उपयोगी बातें सामने आएगी। कृषि पाराशर में दिया हुआ पर्जन्य (वर्षा) का अनुमान, यह सचमुच शोध का विषय हैं। यह अनुमान अगर सत्य हैं, तो अपना सारा कृषि का चित्र बदल सकता हैं। वर्षा के अनुसार फसल लेना यह अपने प्राकृतिक कृषि की प्राचीन संकल्पना हैं। वह ठीक से लागू हो सकेगी।
कुछ वर्ष पहले मैंने ‘वैश्विक गणेश’ यह श्रृंखला लिखी थी। वह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस निमित्त से, ‘विश्व में भगवान श्री गणेश का अस्तित्व, अनेक स्थानों पर हैं’, यह रेखांकित हुआ। वर्तमान में, पूरे विश्व में हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा हैं। इस प्रक्रिया में भगवान गणेश का स्थान कितना महत्व का हैं, यह समझ में आता हैं। पाठकों के आग्रह पर, ‘वैश्विक गणेश’ का समावेश, इस पुस्तक में किया हैं।
यह पुस्तक तैयार करने में अनेकों की मदद हुई। मेरी पत्नी सुमेधा के बिना इस पुस्तक की कल्पना संभव नही थी। उसने न केवल अनेक संदर्भ मुझे उपलब्ध कराएं, वरन् इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में बहुत मदद की। इंद्रनील और निहारिका ने समय निकालकर, मुझे अनेक संदर्भ और ग्रंथ उपलब्ध करवाएं।