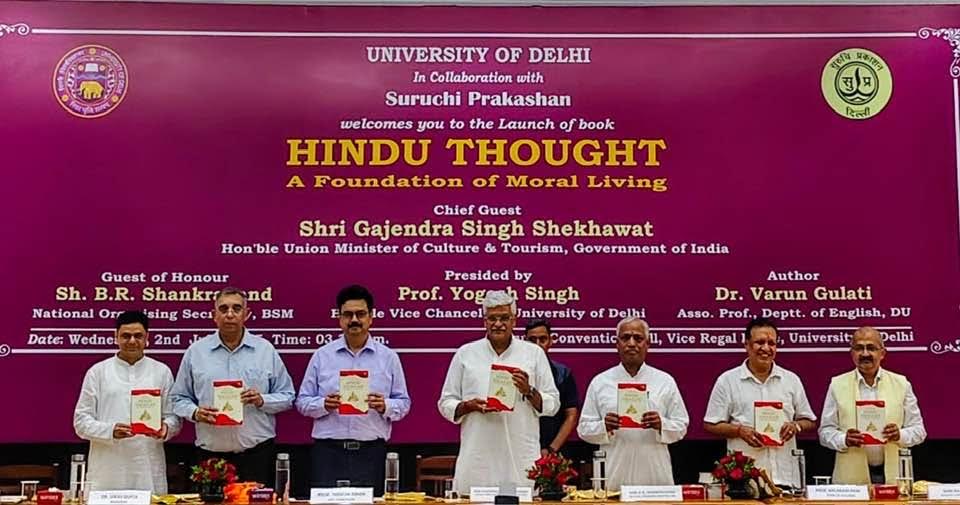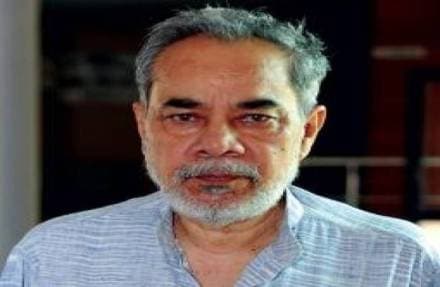कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता यह जानना चाहे कि उसके घर के सामने बनी सड़क के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, वह धन विधायक फंड से आया या किसी अन्य स्रोत से, और उसे किस कंपनी के माध्यम से खर्च किया गया-यह सारी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी जा सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में समय, मेहनत और संसाधनों की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश, बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं का यह समूह धीरे-धीरे थक रहा है। जब समाज में भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल चुकी हो, तो कोई कितने दिन अपनी जमा-पूंजी और ऊर्जा लगाकर परिवर्तन की लड़ाई लड़े? यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जब समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति अपने ही मोहल्ले में दर्जनों दुश्मन बना लेता है। विडंबना यह है कि जिनके लिए वह लड़ रहा होता है, वे अक्सर अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के साथ उठते-बैठते हैं और उसी कार्यकर्ता को दलाल या गलत ठहरा देते हैं।
पटना। बिहार में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पूरे राज्य की पंचायतों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जुटाने का बीड़ा उठाया। इस कार्यकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से हर पंचायत के विकास कार्यों का ब्योरा मांगा, जो स्थानीय मुखिया द्वारा पंचायती फंड से किए गए थे। बिहार का कोई भी नागरिक इस तरह की जानकारी आरटीआई के जरिए प्राप्त कर सकता है। आप भी अपने पंचायत में कितना अैर किस किस मद में खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा मंगा सकते हैं?
लेकिन यह कार्य उतना आसान नहीं था। कार्यकर्ता के लिए ऐसी पंचायत ढूंढना चुनौतीपूर्ण रहा, जहां आवंटित धनराशि के अनुरूप वास्तव में काम हुआ हो। कई जगह कागजों पर सड़कें बन गईं, लेकिन गांव में उनकी मौजूदगी तक नहीं थी। यह आपके गांव का हाल भी हो सकता है? आपने जानकारी इकट्ठी की है क्या?
ऐसे में सवाल उठता है कि जब कागजों पर विकास हो रहा हो और जमीनी हकीकत कुछ और हो, तो न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति न केवल अपनी जेब से खर्च करता है, बल्कि स्थानीय नेताओं और मुखियाओं की दुश्मनी भी मोल लेता है। कई बार वह अपनी लड़ाई में इतना अकेला पड़ जाता है कि सड़क पर चलते चलते कोई ट्रक उसे रौंद कर एक दिन चली जाती है और उसके आस पास के समाज को इससे फर्क तक नहीं पड़ता। या फिर दो चार दिन समाचार पत्रों में चर्चा होती है फिर सब भूल जाते हैं।
जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं, वे अक्सर भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी ले कर चुप्पी साध लेते हैं। यह रास्ता अब लाइजनिंग और वसूली गिरोहों में सबसे प्रचलित है इन दिनों। बिहार के एक चर्चित यू ट्यूबर से जुड़ी ऐसी दर्जनों कहानियां बिहार के लोगों को पता है।
अब उसके समर्थक ही कहते हैं कि ईमानदारी से बिहार के लोगों के लिए लड़ता तो किसी दिन कोई शूटर ठोक कर चला जाता। क्रांतिकारी की इमेज भी बचा ली और दलाली की दूकान भी चल रही है। यही नए दौर की राजनीति है। यह जिसने नहीं सीखा वह राजनीति कर नहीं पाएगा।
बिहार में सुधार की शुरुआत कहां से हो? पंचायतों से, या नगर निगम से जहां एक साल के कार्यकाल में ही मुखिया हो या पार्षद घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी कर लेता है। गांव वाले हों या वार्ड वाले वे सब देखते हैं, लेकिन इस मुद्दे को अपनी बातचीत में शामिल करने से बचते हैं। इसके बजाय, वे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों—जैसे मोदी, राहुल गांधी या ट्रंप की विदेश नीति—पर चर्चा करना पसंद करते हैं। आप समझते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं?
बिहार को राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश माना जाता है, लेकिन यह जागरूकता अक्सर सुरक्षित मुद्दों तक सीमित रहती है। कोई भी स्थानीय स्तर पर मुखिया हो या वार्ड सदस्य की आलोचना करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोग भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के साथ जीना सीख रहे हैं। परिवर्तन की उम्मीद धूमिल हो चुकी है। परिवर्तन की कहानी सुनाकर कोई केजरीवाल अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाने में लग जाता है। अपने परिवार के हेल्थ पर लाखों रुपए साल में खर्च कर रहा है और दिल्ली वालों को मोहल्ला क्लिनिक देकर कहना कि यह विश्वस्तरीय है। यह ठगी ठीक नहीं है।
लोग मानते हैं कि उपलब्ध विकल्पों में मौजूदा नेतृत्व ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए वे उसी के साथ खड़े रहते हैं। धीरे-धीरे समाज में आत्मकेंद्रित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जहां ‘स्व’ का मतलब केवल व्यक्ति, उसकी पत्नी और बच्चे तक सीमित हो गया है। स्व का विकास का अर्थ है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का विकास।
देश और समाज की चिंता अब उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही। इस स्थिति में सवाल यह है कि क्या बिहार में बदलाव संभव है? इसके लिए न केवल जागरूकता, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और साहस की जरूरत है।
आरटीआई जैसे उपकरण सशक्त हो सकते हैं, लेकिन जब तक समाज भ्रष्टाचार को सामान्य मानना बंद नहीं करता, तब तक कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी, यह कहना मुश्किल है।